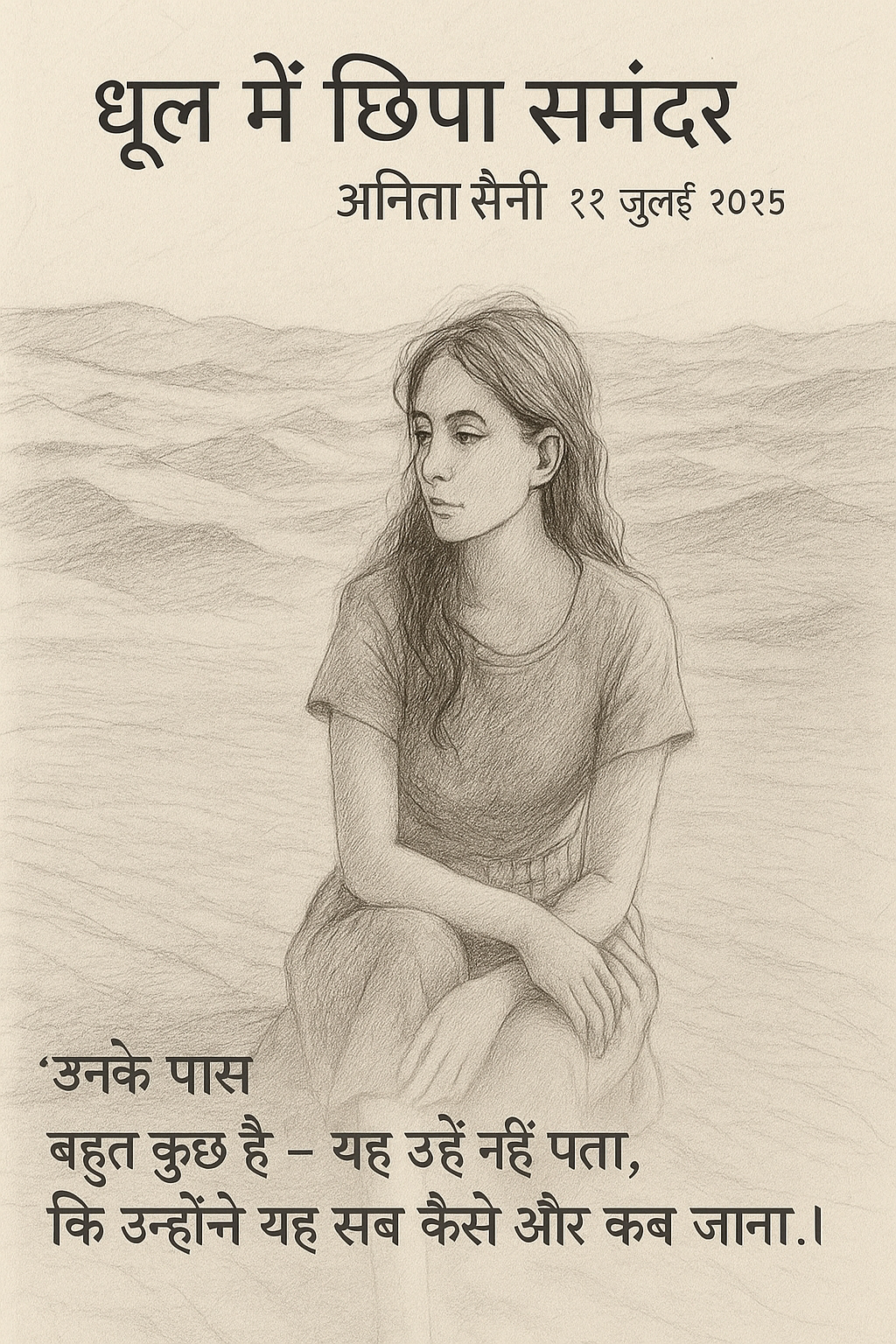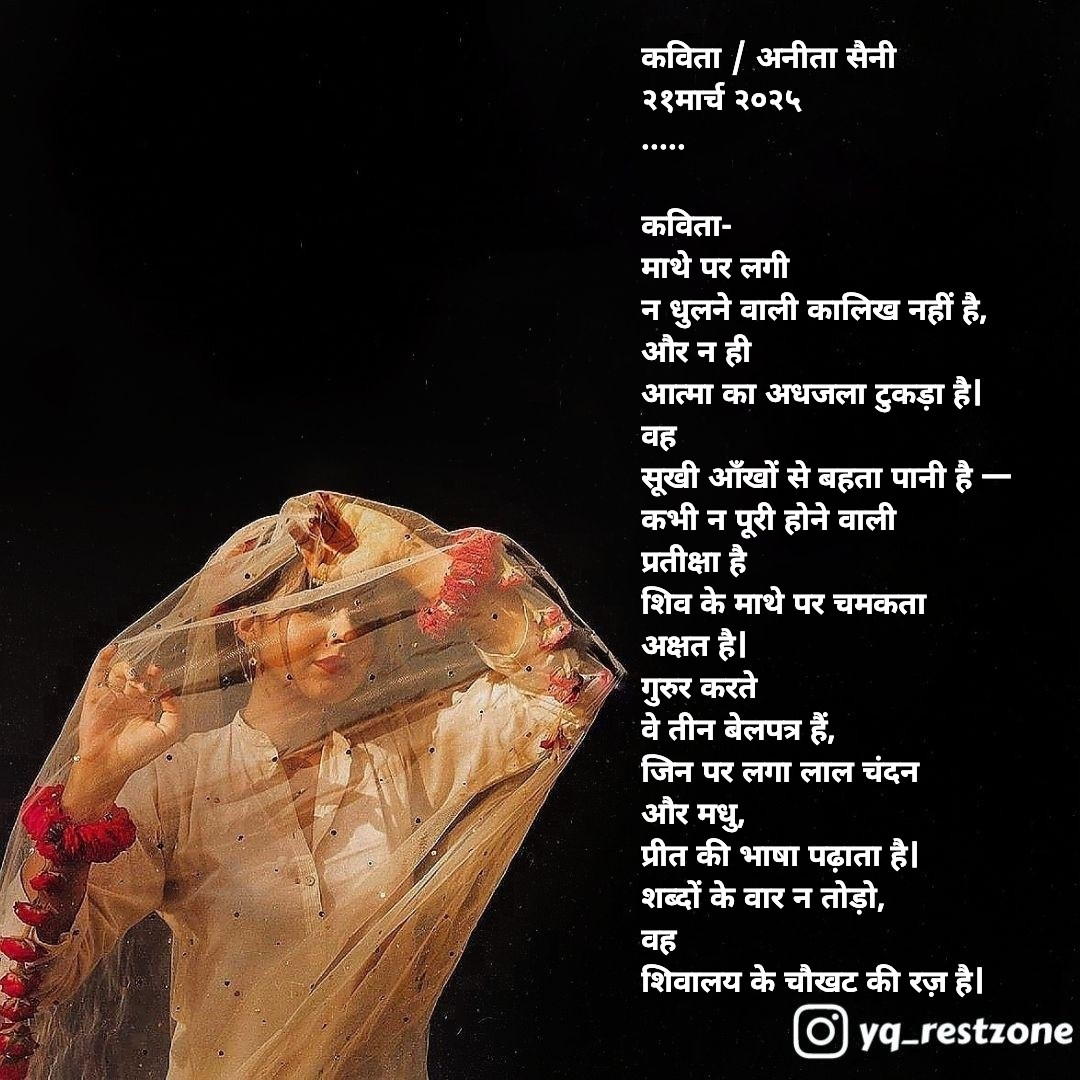सोमवार, दिसंबर 29
ओसरी में खड़ा गवाह
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मंगलवार, दिसंबर 9
प्रतीक्षा एक तीर्थ
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
गुरुवार, दिसंबर 4
भीतर की थिरकन
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मंगलवार, नवंबर 25
रेत पर बिखरे उत्तर
रेत पर बिखरे उत्तर
✍️ अनीता सैनी
…..
कभी
धूप में झिलमिलाते उस सुनसान विस्तार से
दृष्टि मत मोड़ना—
उसका वही एक चकत्ता,
जहाँ पृथ्वी
एड़ियों में अपनी पहली धड़कन
धीरे-धीरे रख देती है।
जो नंगे पाँव उस ताप से गुज़रते हैं,
उनके भीतर
दृढ़ता
रेत के किसी कण-सी
चुपचाप जमने लगती है
पृथ्वी
अपने ही कणों की भाषा में
उन्हें चलना सिखाती है।
क्षितिज पर
नीले जल की पहली झिलमिल
और मन कहता है
नाव की खूँटी ढीली छोड़ दो।
सुरक्षित राहें
कभी नहीं पहुँचातीं वहाँ,
जहाँ पहुँचने की इच्छा
जन्म से साथ चली आती है।
कभी-कभी
एक अनाम हवा
रीढ़ में एक नई रेखा खींच देती है
जैसे समुद्र
अचानक भीतर जाग उठा हो।
लहरें
सबको संकेत नहीं देतीं;
वे उन्हीं तक पहुँचती हैं
जो रस्सियाँ ढीली कर देते हैं
और नाव को
अपने भाग्य के हवाले।
भोर से ठीक पहले
मरुस्थल के होंठों पर
ओस की एक महीन थिति
जिसे कोई नहीं सुनता,
पर वह हर दिन
एक पुरानी प्रार्थना दोहराती है।
दूर
खेजड़ी की दूनी परछाइयाँ
धूप के हर कौर को पीकर
अंदर कहीं
छिपा लेती हैं हरियाली।
पक्षी
किरणों के किनारे से
थोड़ी-सी छाया चुनते हैं
और उसकी नमी से
अपने भीतर
नए पंख उगा लेते हैं।
मैं—
इस शांत विस्तार के बीच
क्षणभर रुककर
बस अनुमति माँगता हूँ
कि थोड़ी देर
धरती के पास बैठ सकूँ।
मेरे पास
कोई इच्छा नहीं
सिर्फ एक ऐसी थकान,
जो विश्राम से इनकार करती है,
जब तक उसे
उसकी उपस्थिति की गर्मी
न मिल जाए।
धीमी धूप
कंधों पर उतरती है।
ओस
पलक से फिसलकर
रेत में समा जाती है।
और तभी समझ आता है
मिट्टी ने
अपने मौन में
बहुत पहले
सारे उत्तर लिख रखे थे।
तब मैं
अपने ही प्रश्नों को देख
मुस्कुरा देता हूँ।
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
रविवार, नवंबर 16
नदी का छिपा हुआ दीप
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
रविवार, नवंबर 2
रेत भी प्रेम में उतरती है
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
बुधवार, अक्टूबर 22
जड़ में जीवन है
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
रविवार, अक्टूबर 12
शैवाल से शिला तक
शैवाल से शिला तक
✍️ अनीता सैनी
—
वह समय —
जो कभी नहीं लौटता,
जिसका अब जीवन में कोई औचित्य नहीं,
वही सबसे अधिक बुलावा भेजता है;
कोस मीनार-सा खड़ा,
अनुगूंज बनकर कहता है —
मेरी नाड़ी में अब भी
एक अनसुनी प्रतीक्षा धड़कती है।
मैं अब भी यहीं हूँ —
जहाँ शब्द थम जाते हैं,
और दृष्टि
प्रतीक्षा के जल में
अपना प्रतिबिंब टटोलती है।
वर्षों से थामी इस डोर का सिरा,
विश्वास की नमी में भीगा है,
पर टूटा नहीं —
बस समय की उँगलियों में
उलझा पड़ा है।
और कहता है —
प्रतीक्षा सूखती नहीं अंत में,
ढूँढती है कि
क्या कोई अब भी वहाँ है,
जहाँ से वह चला था।
जहाँ —
समय की साँसों पर
स्मृतियों के शैवाल उग आए हैं;
वे शैवाल,
हरे हैं — पर थके हुए,
जो अब धीरे-धीरे
एक कोरी
शिला बनते जा रहे हैं।
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
गुरुवार, अक्टूबर 9
मौन का शास्त्र
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
गुरुवार, अक्टूबर 2
सूखा कुआँ
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
शुक्रवार, सितंबर 26
चेतना का मानचित्र
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
शनिवार, सितंबर 20
प्रतीक्षा में खड़ी हूँ
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
रविवार, सितंबर 14
नमी की आवाज़
नमी की आवाज़
✍️ अनीता सैनी
दुपहर अब भी दूरियों को खुरचती है,
बादलों ने करवट नहीं बदली—
फिर भी बरसात उतर आती है।
वे पगडंडियाँ जंगल तक नहीं पहुँचतीं,
पेड़ पानी पीकर
नदियों की प्यास भुला देते हैं।
ओसारे में टपकती बोरियाँ
भीतर रखे दाने भिगो देती हैं।
दीवारों से सीलन रिसती है,
कोनों का दिया बुझकर
धुआँ छोड़ जाता है।
दिन—
आँगन में भीगी लकड़ियाँ समेटता है।
साँझ—
कागज़ का थैला सँभालते हुए
अनाज के संग
समय का भार भी ढोती है।
भूल जाते हैं सब—
गली के उस मोड़ पर
वही कौआ काँव-काँव करता है।
पाँवों के निशान मिटते नहीं,
मिट्टी में धँसकर
अस्तित्व की जड़ों में बदल जाते हैं।
हवा खिड़कियाँ झकझोरती है,
चूल्हे की हांडी उबलकर
घर की निस्तब्धता को गूँज में बदल देती है।
बरामदे के पौधे
अधिक पानी पीकर झुक जाते हैं—
मानो विनम्रता का भार उठाए हों।
रात के हाथ
आटे में भीगकर सफेद हो जाते हैं।
सन्नाटा
अपनी थाली बजाकर याद दिलाता है—
कि बरसात अब भी होती है।
और तुम्हारे पाँव हैं कि —
पराई धरती पर भी
अपनी मिट्टी खोज लेते हैं।
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
सोमवार, सितंबर 8
अस्तित्व का बहना
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
गुरुवार, सितंबर 4
अधूरेपन का आकाश
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
शुक्रवार, अगस्त 29
धुँधलों से हरापन
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
शनिवार, अगस्त 23
कल्पना की चुप्पी
✍️ अनीता सैनी
...
और कुछ नहीं—
बस ठठा उठता है वह पल,
जब दरिद्र हो जाती है मेरी कल्पना,
मानो चेतना का स्रोत ही
क्षण भर में सूख गया हो।
शब्दों का अंबार होते हुए भी
विचार रिक्त खड़े रह जाते हैं—
जैसे मानो
मौन ही आखिरी सत्य बनकर
हर तर्क और हर अभिव्यक्ति को
अर्थहीन कर देता है।
मैं लिखना चाहूँ भी तो
शब्द ठिठक जाते हैं,
क्योंकि सामने तुम्हारा प्रतिबिंब है—
जो मेरे अल्प विचारों की सीमा को
छिन्न-भिन्न कर देता है,
और मेरे भावों को उस
अनन्त के सामने लज्जित कर देता है।
मेरी पंक्तियों में जितना समा पाता है,
उससे कहीं अधिक विराट
व्यथा का प्रतिबिंब
कल्पना के दर्पण में झलक उठता है—
जहाँ कोनों की कोरी चुप्पी
तुम्हारी प्रतीक्षा में
बिलखती रह जाती है।
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
शनिवार, जुलाई 12
धूल में छिपा समंदर
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
सोमवार, जून 30
छलावा
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
शुक्रवार, जून 20
दरकन
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
गुरुवार, जून 19
मीरा — एक अंतरध्वनि
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
रविवार, जून 1
कोख से कंठ तक
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
बुधवार, अप्रैल 23
स्मृति के छोर पर
२२ अप्रैल २०२५
….
अपने अस्तित्व से मुँह फेरने वाला व्यक्ति,
उस दिन
एक बार फिर जीवित हो उठता है,
जब वह धीरे-धीरे
अपने अब तक के, जिए जीवन को
भूलने लगता है।
उसे समझ होती है तो बस इतनी कि
धीरे-धीरे भूलना
और
अचानक सब कुछ भूल जाना —
इन दोनों में अंतर है।
एक जीवन है,
तो दूसरा मृत्यु।
उसे जीवन मिला है —
वह धीरे-धीरे स्वयं को भूल रहा है,
क्योंकि वह अब भी
भोर को ‘भोर’ के रूप में पहचानता है।
जब वह सुबह उठता है,
तो वह
सुबह को ‘सुबह’ के रूप में पहचानता है।
वह
‘न पहचान पाने’ की पीड़ा को भी पहचानता है।
वह दिन में नहीं सोता —
इस डर से नहीं कि रात को उठने पर
कहीं वह रात को
‘रात’ के रूप में पहचान न पाया तो,
बल्कि इसलिए
कि वह
दिन को ‘दिन’ के रूप में पहचानता है,
और स्वयं को पुकारता है
टूटती पहचान की अंतिम दीवार की तरह।
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
शनिवार, अप्रैल 19
नीरव सौंदर्य
१८अप्रैल २०२५
….
आश्वस्त करती
अनिश्चितताएँ जानती हैं!
घाटियों में आशंकाएँ नहीं पनपतीं;
वहाँ
मिथ्या की जड़ें
गहरी नहीं, अपितु कमजोर होती हैं।
वहाँ अंखुए फूटते हैं
उदासियों के।
जब उदासियाँ
घाटियों में बैठकर कविताएँ रचती हैं,
तब उनके पास
केवल चमकती हुई दिव्य आँखें ही नहीं होतीं,
अपार सौंदर्य भी होता है।
नाक, सौंदर्य का एक अनुपम उदाहरण है,
जिसकी रक्षा आँखें आजीवन करती हैं।
वे यूँ ही नहीं कहतीं—
"कविता प्यास है न हीं तृप्ति
बस
एक घूंट पानी है।"
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
सोमवार, अप्रैल 14
प्रतीक्षा का अंतिम अक्षर
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मंगलवार, मार्च 25
तुम कह देना
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
सोमवार, मार्च 24
कविता
कविता-
माथे पर लगी
न धुलने वाली कालिख नहीं है,
और न ही
आत्मा का अधजला टुकड़ा है।
वह
सूखी आँखों से बहता पानी है —
कभी न पूरी होने वाली
प्रतीक्षा है
शिव के माथे पर चमकता
अक्षत है।
गुरुर करते
वे तीन बेलपत्र हैं,
जिन पर लगा लाल चंदन
और मधु,
प्रीत की भाषा पढ़ाता है।
शब्दों के वार न तोड़ो,
वह
शिवालय के चौखट की रज़ है।
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
सोमवार, फ़रवरी 17
निराशा का आत्मलाप
निराशा का आत्मलाप / अनीता सैनी
१६फरवरी २०२४
….
उबलता डर
मेरी नसों में
अब भी
सांसों की गति से तेज़ दौड़ रहा है,
जो कई रंगों में रंगा,
चकत्तों के रूप में
मेरी आँखों में उभर-उभर कर
आ रहा है।
आँखों से संबंधित रोग की तरह,
जो
मेरी काया को धीरे-धीरे ठंडा कर रहा है
और आत्मा को गहरे शून्य में डुबो रहा है।
अलविदा—
गहरे कोहरे में हिलता हाथ,
या जैसे
कोई समंदर के बीचो-बीच
डूबता हुआ एक हाथ।
मुझे पता है,
यह एक कछुए का हाथ है,
परंतु
ये मेरे वे निराशाजनक दृश्य हैं,
जिन्हें मुझे अकेले ही जीना है।
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
रविवार, जनवरी 19
अधूरे सत्य की पूर्णता
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
सोमवार, जनवरी 13
बालिका वधू
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
रविवार, जनवरी 5
बुकमार्क
बुकमार्क / अनीता सैनी
३जनवरी २०२५
……
पुस्तक —
प्रभावहीन शीर्षक,
आवरण, तटों को लाँघती नदी,
फटा जिल्द,
शब्दों में
उभर-उभरकर आता ऋतुओं का पीलापन,
कुछ पन्नों के बाद
पाठक द्वारा लगाया बुकमार्क
उसे रसहीन बताता रहा।
पुस्तक के अनछुए पन्ने,
व्यवस्थित रहने का सलीका ही नहीं,
मौन में मधुर स्मृतियों को पीना सिखाते रहे।
उसे बार-बार हिदायत देते रहे—
न पढ़ पाने की पीड़ा में
न अधिक चिल्लाकर रोना है,
और न ही
ठहाका लगाकर हँसना है।
चेतावनी—
सिले होठों से भाव अधिक मुखर होते हैं।
इतने शालीन ढंग से टिके रहना,
कि समय
पन्नों से हवा के ही नहीं,
आँधियों के भी आँसू पोंछ सके।
पुस्तक—
कोने में
स्वयं को पढ़ती है, पढ़ती है
तटों को तोड़ती एक-एक धारा को।
उसे न पढ़ पाने की पीड़ा नहीं कचोटती,
कचोटता है—
बिना पढ़े लगाया बुकमार्क।
 मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |
मैं एक ब्लॉगर हूँ, स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हूँ, प्रकृति के निकट स्वयं को पाकर रचनाएँ लिखती हूँ, कविता भाव जगाएँ तो सार्थक है, अन्यथा कविता अपना मर्म तलाशती है |